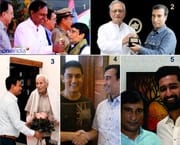श्री यशवंत कोठारी
(वरिष्ठ साहित्यकार श्री यशवन्त कोठारी जी का ई-अभिव्यक्ति में स्वागत। आपके लगभग 2000 लेख, निबन्ध, कहानियाँ, आवरण कथाएँ, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सारिका, नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, नवज्योती, राष्ट्रदूत साप्ताहिक, अमर उजाला, नई दुनिया, स्वतंत्र भारत, मिलाप, ट्रिव्यून, मधुमती, स्वागत आदि में प्रकाशित/ आकाशवाणी / दूरदर्शन …इन्टरनेट से प्रसारित। अमेज़न Kindle, Pocket FM .in पर ऑडियो बुक्स व् Matrubharati पर बुक्स उपलब्ध। 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित। सेमिनार-कांफ्रेस:– देश-विदेश में दस राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आमंत्रित / भाग लिया। राजस्थान साहित्य अकादमी की समितियों के सदस्य 1991-93, 1995-97, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की राजभाषा समिति के सदस्य-2010-14.)
☆ व्यंग्य ☆ श्वान और मालिक का प्रात: कालीन भ्रमण… ☆ श्री यशवंत कोठारी ☆
रोज़ सुबह इस पोश कोलोनी में घूमने के साथ साथ कई काम एक साथ हो जाते हैं. कचरा फेंक देता हूँ दूध ले आता हूँ, गाय को रोटी दे आता हूँ और घूम भी लेता हूँ. बड़े लोग, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियाँ और छोटे छोटे दिल लेकिन बड़े बड़े पेट्स इनको श्वान या कुत्ता कहना मालिक या मालकिन का अपमान है.
अक्सर मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग याद आता है जिसमे वे एक सुबह घूमने वाले को देख कर कहते हैं –इस गधे के साथ कहाँ जा रहें हैं पेट- मालिक बोलता है –यह गधा नहीं मेरा पेट डॉग है अमित जी मासूमियत से कहते हैं मैंने यह सवाल आप से नहीं पेट से ही पूछा था. खैर छोडिये.
अब तो अदालत ने भी गली मोहल्लों के कुत्तों के लिए स्थान सुनिश्चित करने को बोला है कोलोनी वाले उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करेंगे. अब तो पेट डॉग्स के लिए पार्क भी बनने लग गए हैं. पेट ट्रेनर की रेट कोचिंग से भी ज्यादा हो गयी है, घुमाने के लिए स्टाफ रखा जाता है. सुबह पेट को घुमाने वाले उसे पट्टे से आजाद कर के खुला छोड़ देते हैं, पेट अपना पेट साफ कर लेता है सुसु से धरा को पवित्र कर देता है तब तक मालिक दूर खड़ा रहता है ताकि आक्षेप करने पर यह कह सके की यह पेट मेरा नहीं है, निवृत्त हो कर पेट मालिक के पास आ जाता है मालिक उसे पट्टे से बांध कर घर की और चल देता है. कुछ समझदार पेट मालिक अपने श्वान की पोट्टी थेली में भर कूड़े दान में डाल देते हैं अपनी संतानों की नेपि भले न बदली मगर पेट के लिए कर देते हैं. कॉलोनी में पेट्स का सामना अक्सर आवारा कुत्तों से हो जाता है गली के श्वान बंगले के श्वान से सेमिनार और वर्कशॉप करने लग जाते हैं इस सामूहिक रुदन से देर से उठने वाले परेशान हो जाते हैं, मगर विरोध करने पर पशुप्रेमी स्वयं सेवी संस्था के महारथी लोग आ जाते हैं और आवारा कुत्तों को उठाने वाली गाड़ी के आगे लेट जाते हैं स्थिति हर गली मोहल्ले में एक जैसी है. श्वान प्रेमी होना अच्छा है लेकिन क्या मानवतावादी होना गलत है, हर शहर में नवजात बच्चों, बूढों बुजुर्गों, महिलाओं को ये श्वान अपना शिकार बना चुके हैं एक दान्त गड़ने पर दस हज़ार का मुआवजा देने के आदेश है लेकिन ऐसी स्थिति ही क्यों आये ?
पेट पालें, मगर दूसरों की जिन्दगी से खिलवाड़ न करें. कुत्तों के अलावा बिल्ली, तोता, चिड़िया, खरगोश, कछुआ या अन्य जानवर पाले जा सकते हैं. आवारा जानवरों के खतरें बहुत है. सड़क पर रा त- बिरात निकलना तक मुश्किल हो गया है श्रीमान. पेट्स के भी खान दान होते हैं असली नस्ल को पहचानने के लिए विशेषज्ञ है, नस्ल सुधारने वाले भी मिल जाते हैं. लेकिन मानव की कौन सोचता है? कुत्ते नवजात तक भी पहुँच जाते हैं. चीर फाड़ देते हैं, लेकिन कौन सुनता है ?
डॉग के सामानों की दुकानें हैं और वहां पर खरीदारों की भीड़ भी है, विदेशों मे तो अलग से पूरे बाज़ार है भारत में भी खुलने की प्रक्रिया है लेकिन आम राहगीर, पैदल चलने वाले, सुबह घूमने के शौक़ीन लोग इस पेट प्यार से दुखी परेशान है. नगर निगम सुनता नहीं कभी सुन ले तो एन जी ओ चलाने वाले पशु प्रेमी गाड़ी को घेर कर कुत्तों को छुड़ा लेते हैं. उनका प्रेम आवारा जानवरों के प्रति नहीं उमड़ता है गरीब दलित आदिवासी के लिए भी नहीं केवल पेट प्यार के मारे हैं ये सब. हजारों लोग हर साल कुत्तों के काटने से मर जाते हैं, कुत्ता नियंत्रण क़ानून बना है लेकिन इस से क्या होता है ? पेट मालिक पर मुकदमें चलाये जाने चाहिए. आंकड़ों के अनुसार रेबीज से हर साल हजारों लोग घायल होते हैं या मर जाते हैं
पेट मालिकों को दूसरों की जिन्दगी से खेलने का कोई ह़क नहीं हैं, सुनो क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंचती है ?
☆
© श्री यशवन्त कोठारी
संपर्क – 701, SB-5, भवानी सिंह रोड, बापू नगर, जयपुर -302015 मो. -94144612 07
≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ≈