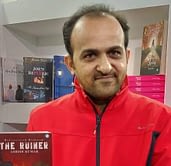डॉ. मुक्ता
(डा. मुक्ता जी हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक एवं माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत हैं। साप्ताहिक स्तम्भ “डॉ. मुक्ता का संवेदनात्मक साहित्य” के माध्यम से आप प्रत्येक शुक्रवार डॉ मुक्ता जी की उत्कृष्ट रचनाओं से रूबरू हो सकेंगे। आज प्रस्तुत है डॉ मुक्ता जी का जीवन में चिंता का स्थान एवं उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करता एकआलेख चिंता बनाम पूजा।यह डॉ मुक्ता जी के जीवन के प्रति गंभीर चिंतन का दस्तावेज है। डॉ मुक्ता जी की लेखनी को इस गंभीर चिंतन से परिपूर्ण आलेख के लिए सादर नमन। कृपया इसे गंभीरता से आत्मसात करें। )
☆ साप्ताहिक स्तम्भ – डॉ. मुक्ता का संवेदनात्मक साहित्य # 46 ☆
☆ चिंता बनाम पूजा ☆
‘जब आप अपनी चिंता को पूजा, आराधना व उपासना में बदल देते हैं, तो संघर्ष दुआओं में परिवर्तित हो जाता है।’ चिंता तनाव की जनक व आत्मकेंद्रिता की प्रतीक है, जो हमारे हृदय में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। इसके कारण ज़माने भर की ख़ुशियाँ, हमें अलविदा कह रुख़्सत हो जाती हैं और उसके परिणाम-स्वरूप हम घिर जाते हैं–चिंता, तनाव व अवसाद के घने अंधकार में–जहां हमें मंज़िल तक पहुंचाने वाली कोई भी राह नज़र नहीं आती।’
वैसे भी चिंता को चिता समान कहा गया है, जो हमें कहीं का नहीं छोड़ती और हम नितांत अकेले रह जाते हैं। कोई भी हमसे बात तक करना पसंद नहीं करता, क्योंकि सब सुख के साथी होते हैं और दु:ख में तो अपना साया तक भी साथ नहीं देता। सुख और दु:ख एक-दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु हैं। एक की अनुपस्थिति में ही दूसरा दस्तक देने का साहस जुटा पाता है…तो क्यों न इन दोनों का स्वागत किया जाए। ‘अतिथि देवो भव’ हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, आस्था है, विश्वास है, जो सुसंस्कारों से पल्लवित व पोषित होता है। आस्था व श्रद्धा से तो धन्ना भगत ने पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया था। हां! जब हम चिंता को पूजा में बदल लेते हैं अर्थात् सम्पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तो वह प्रभु की चिंता बन जाती है, क्योंकि वे हमारे हित के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। सो! आइए–अपनी चिंताओं को उस सृष्टि-नियंता को समर्पित कर सुक़ून से ज़िंदगी बसर करें।
‘बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय’ इस कहावत से तो आप सब परिचित होंगे कि जिस मनुष्य पर प्रभु का वरद्-हस्त रहता है, उसे कोई लेशमात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता; उसका अहित नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं कि अब तो सब कुछ प्रभु ही करेगा। जो भाग्य में लिखा है, अवश्य होकर अर्थात् मिल कर रहेगा क्योंकि ‘कर्म गति टारे नहीं टरहुं।’ गीता मेंं भी भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म का संदेश दिया है तथा उसे ‘सार्थक कर्म’ की संज्ञा दी है। उसके साथ ही वे परोपकार का संदेश हुए, मानव-मात्र के हितों का ख्याल रखने को कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे हाशिये के उस पार के नि:सहाय लोगों के लिए मंगल-कामना करते हैं, ताकि समाज में सामंजस्यता व समरसता की स्थापना हो सके। वास्तव में यही है–सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम राह, जिस पर चल कर हम कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
संघर्ष को दुआओं में बदलने की स्थिति जीवन में तभी आती है, जब आपके संघर्ष करने से दूसरों का हित होता है और असहाय व पराश्रित लोग अभिभूत हो, आप पर दुआओं की वर्षा करनी प्रारंभ कर देते हैं। दुआ दवा से भी अधिक श्रेयस्कर व कारग़र होती है, जो मीलों का फ़ासला पल भर में तय कर प्रार्थी तक पहुंच अपना करिश्मा दिखा देती है तथा उसका प्रभाव अक्षुण्ण होता है…रेकी भी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आजकल तो वैज्ञानिक भी गायत्री मंत्र के अलौकिक प्रभाव देख कर अचंभित हैं। वे भी इस तथ्य को स्वीकारने लगे हैं कि दुआओं व वैदिक मंत्रों में विलक्षण व अलौकिक शक्ति होती है। मुझे स्मरण हो रही हैं– स्वरचित मुक्तक-संग्रह ‘अहसास चंद लम्हों का’ की चंद पंक्तियां… जो जीवन मे अहसासों की महत्ता व प्रभुता को दर्शाती हैं… ‘अहसास से रोशन होती है ज़िंदगी की शमा/ अहसास कभी ग़म, कभी खुशी दे जाता है/ अहसास की धरोहर को सदा संजोए रखना/ अहसास ही इंसान को बुलंदियों पर पहुंचाता है।’ अहसास व मन के भावों में असीम शक्ति है, जो असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखते हैं।
उक्त संग्रह की यह पंक्तियां सर्वस्व समर्पण के भाव को अभिव्यक्त करती है…’मैं मन को मंदिर कर लूं /देह को मैं चंदन कर लूं /तुम आन बसो मेरे मन में /मैं हर पल तेरा वंदन कर लूं’…जी हां! यह है मानसिक उपासना… जहां मैं और तुम का भाव समाप्त हो जाता है और मन, मंदिर हो जाता है और भक्त को प्रभु को तलाशने के लिए मंदिर-मस्जिद व अन्य धार्मिक-स्थलों में माथा रगड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। उसकी देह चंदन-सम हो जाती है, जिसे घिस-घिस कर अर्थात् जीवन को साधना में लगा कर, वह प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहता है। उसकी एकमात्र उत्कट इच्छा यही होती है कि परमात्मा उसके मन में रच-बस जाए और वह हर पल उसका वंदन करता रहे… एक भी सांस बिना सिमरन के व्यर्थ न जाए। इसी संदर्भ में मुझे स्मरण हो रहा है–महाभारत का वह प्रसंग, जब भीष्म पितामह शर-शैय्या पर लेटे थे। दुर्योधन पहले आकर उनके शीश की ओर स्थान प्राप्त कर स्वयं को गर्वित व हर्षित महसूसता है और कृष्ण उनके चरणों में बैठ कर संतोष का अनुभव करते हैं। सो! वह कृष्ण से प्रसन्नता का कारण पूछता है और अपने प्रश्न का उत्तर पाकर हतप्रभ रह जाता है कि ‘मानव की दृष्टि सबसे पहले सामने वाले अर्थात् चरणों की ओर बैठे व्यक्ति पर पड़ती है, शीश की ओर बैठे व्यक्ति पर नहीं।’ भीष्म पितामह भी पहले कृष्ण से संवाद करते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मेरी दृष्टि तो पहले वासुदेव कृष्ण पर पड़ी है। इससे संदेश मिलता है कि यदि तुम जीवन.में ऊंचाई पाना चाहते हो, तो अहं को त्याग, विनम्र बन कर रहो, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़कर रहता है; फलदार वृक्ष की भांति झुक कर रहता है… सदैव उन्नति के शिखर पर पहुंच सूक़ून व प्रसिद्धि पाता है।’
सो! प्रभु का कृपा-प्रसाद पाने के लिए उनकी चरण-वंदना करनी चाहिए… जो इस कथन को सार्थकता प्रदान करता है कि ‘यदि तुम जीवन में ऊंचाई पाना चाहते हो अथवा उन्नति के शिखर को छूना चाहते हो, तो किसी काम को छोटा मत समझो। जीवन में खूब परिश्रम करके सदैव नंबर ‘वन’ पर बने रहो और उस कार्य को इतनी एकाग्रता व तल्लीनता से करो कि तुम से श्रेष्ठ कोई कर ही न सके। सदैव विनम्रता का दामन थामे रखो, क्योंकि फलदार वृक्ष व सुसंस्कृत मानव सदैव झुक कर ही रहता है।’ सो! अहं मिटाने के पश्चात् ही आपको करुणा-सागर के निज़ाम में प्रवेश पाने का सुअवसर प्राप्त होगा। अहंनिष्ठ मानव का वर्तमान व भविष्य दोनों अंधकारमय होते हैं। वह कहीं का भी नहीं रहता…न वह इस लोक में सबका प्रिय बन पाता है, न ही उसका भविष्य संवर सकता है अर्थात् उसे कहीं भी सुख-चैन की प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए भारतीय संस्कृति में नमन को महत्व दिया गया है अर्थात् अपने मन से नत अथवा झुक कर रहिए, क्योंकि अहं को विगलित करने के पश्चात् ही मानव के लिए प्रभु के चरणों में स्थान पाना संभव है। नमन व मनन दोनों का संबंध मन से होता है। नमन में मन से पहले न लगा देने से और मनन में मन के पश्चात् न लगा देने से मनन बन जाता है। दोनों स्थितियों का प्रभाव अद्भुत व विलक्षण होता है, जो मानव को कैवल्य की ओर ले जाती हैं। सो! नमन व मनन वही व्यक्ति कर पाता है, जिसका अहं अथवा सर्वश्रेष्ठता का भाव विगलित हो जाता है और वह विनम्र.प्राणी निरहंकार की स्थिति में आकाश की बुलंदियों को छूने का सामर्थ्य रखता है।
‘यदि मानव में प्रेम, प्रार्थना व क्षमा भाव व्याप्त हैं, तो उसमें शक्ति, साहस व सामर्थ्य स्वत: प्रकट हो जाते हैं, जो जीवन को उज्ज्वल बनाने में सक्षम हैं।’ इसलिए सब से प्रेम करने से सहयोग व सौहार्द बना रहेगा और आपके ह्रदय में प्रार्थना भाव जाग्रत हो जायेगा …आप मानव-मात्र के हित व मंगल की कामना करना प्रारंभ कर देंगे। इस स्थिति में अहं व क्रोध का भाव विलीन हो जाने पर करुणा भाव जाग्रत हो जाना स्वाभाविक है। महात्मा बुद्ध ने भी प्रेम, करुणा व क्षमा को सर्वोत्तम भाव स्वीकारते हुए, क्षमा भाव को क्रोध पर नियंत्रित करने के अचूक साधन व उपाय के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। इन परिस्थितियों में मानव शक्ति व साहस के होते हुए भी, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर, निर्बल पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करता, क्योंकि वह ‘क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात’ अर्थात् वह बड़ों में क्षमा भाव की उपयोगिता, आवश्यकता, सार्थकता व महत्ता को समझता-स्वीकारता है। महात्मा बुद्ध भी प्रेम व करुणा का संदेश देते हुए स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में ‘जब आप शक्तिशाली होते हुए भी निर्बल पर प्रहार नहीं करते, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है।’ इसके विपरीत यदि आप में शत्रु का सामना करने की सामर्थ्य व शक्ति ही नहीं है, तो चुप रहना आप की विवशता है, मजबूरी है, करुणा नहीं। मुझे स्मरण हो रहा है, शिशुपाल प्रसंग …जब शिशुपाल ने क्रोधित होकर भगवान कृष्ण को 99 बार गालियां दीं और वे शांत भाव से मुस्कराते रहे। परंतु उसके 100वीं बार वही सब दोहराने पर उन्होंने उसके दुष्कर्मों की सज़ा देकर उसके अस्तित्व को मिटा डाला।
सो! कृष्ण की भांति क्षमाशील बनिए। विषम व विपरीत परिस्थितियों में धैर्य का दामन थामे रखें, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया देने से जीवन में केवल तनाव की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती, बल्कि ज्वालामुखी पर्वत की भांति विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी जीवन में सुनामी जीवन की समस्त खुशियों को लील जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए उस स्थान को त्यागना श्रेयस्कर है, क्योंकि क्रोध तो दूध के उफ़ान की भांति पूर्ण वेग से आता है और पल-भर में शांत हो जाता है। सो! जीवन में अहं का प्रवेश निषिद्घ कर दीजिए …क्रोध अपना ठिकाना स्वत: बदल लेगा।
वास्तव में दो वस्तुओं के द्वंद्व अर्थात् अहं के टकराने से संघर्ष का जन्म होता है। सो! पारिवारिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अहं का त्याग अपेक्षित है, क्योंकि संघर्ष व टकराव से पति-पत्नी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका खामियाज़ा बच्चों को एकांत की त्रासदी के दंश रूप में झेलना पड़ता है। सो! संयुक्त परिवार-व्यवस्था के पुन: प्रचलन से जीवन में खुशहाली छा जाएगी। सत्संग, सेवा व सिमरन का भाव पुन: जाग्रत हो जाएगा अर्थात् जहां सत्संगति है, सहयोग व सेवा भाव अवश्य होगा, जिसका उद्गम-स्थल समर्पण है। सो! जहां समर्पण है, वहां अहं नहीं; जहां अहं नहीं, वहां क्रोध व द्वंद्व नहीं– टकराव नहीं, संघर्ष नहीं; क्योंकि द्वंद्व ही संघर्ष का जनक है। यह स्नेह, प्रेम, सौहार्द, त्याग, विश्वास, सहनशीलता व सहानुभूति के दैवीय भावों को लील जाता है और हम चिंता, तनाव व अवसाद के मकड़जाल में फ़स कर रह जाते हैं… जो हमें जीते-जी नरक के द्वार तक ले जाते हैं। आइए! चिंता को त्याग व अहं भाव को मिटा कर, पूर्ण समर्पण करें, ताकि संघर्ष दुआओं में परिवर्तित हो जाए और जीते-जी मुक्ति प्राप्त करने की राह सहज व सुगम हो जाए।
© डा. मुक्ता
माननीय राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत।
पूर्व निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, #239,सेक्टर-45, गुरुग्राम-122003 ईमेल: drmukta51@gmail.com
मो• न•…8588801878